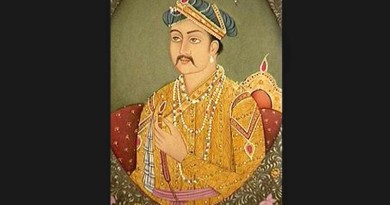केंद्र-राज्यों के बीच विवादस्पद मुद्दे The Controversial Issues Between States And The Union
प्रशासनिक एवं विधायी विषय
अनुच्छेद 356 एवं 355 का दुरुपयोग
केंद्र द्वारा संविधान के अनुच्छेद-356 का दुरुपयोग राज्य विधानसभा को भंग करने के लिए बार-बार किया जाता है, जो संघीय सिद्धांत एवं राज्यों के अधिकारों के लिए घातक बनता जा रहा है। अंतरराज्यीय परिषद् की लगातार बैठकों में विभिन्न वर्गों से अनुच्छेद- 356 के प्रयोग को ऐसे मामलों तक सीमित करने की मांग उठती रही है, जहां देश की राष्ट्रीय एकता या धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को गंभीर खतरा पैदा हो गया हो। अनुच्छेद-355 को स्पष्ट करने की आवश्यकता है।
राज्यपाल की नियुक्ति एवं भूमिका
केंद्र द्वारा राज्यों के लिए नियुक्त राज्यपाल का प्रावधान अराजकतापूर्ण रहा है, जो संघीय लोकतांत्रिक राजव्यवस्था के अनुरूप नहीं है। विश्व में कहीं भी किसी बड़े देश में राज्यों के लिए केंद्र द्वारा राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है। राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी की समय सीमा भी निश्चित होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्यपाल पर राज्य सरकार से खुले तौर पर असहमति एवं मतभेद व्यक्त करने को रोकने हेतु मापदंड होना चाहिए।
राज्य सूची पर केंद्र का दखल: इस बात की त्वरित समीक्षा करने की आवश्यकता है कि राज्य सूची से विधायी मामलों की संघ/समवर्ती सूची को स्थानांतरित करने के क्या प्रभाव होंगे। न केवल शिक्षा जैसे विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डालने से, अपितु तथाकथित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में तीव्र वृद्धि द्वारा भी केंद्र सरकार ने राज्य सूची में घुसपैठ की है। राज्य विषयों पर ये केंद्रीय योजनाएं, जिनमें केंद्र द्वारा लगाए गये कठोर निर्देश होते हैं, वित्तीय निहितार्थों के अतिरिक्त राज्य की स्वायत्तता एवं उनके विकास अधिमानताओं को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त, समवर्ती सूची के तहत् विषयों के क्षेत्रों पर संघ-राज्य के बीच परामर्श करने का कोई औपचारिक संस्थागत ढांचा नहीं है।
संधि करने की शक्ति: संधि करने की शक्ति के संबंध में वर्तमान संविधानिक योजना, जो विशिष्ट रूप से संघीय कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है, पर तुरंत समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय संधि के लिए विधायी प्रतिबंध लगाने पर संविधान में संशोधन किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, विश्व व्यापार संगठन समझौते जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां राज्यों के लिए गंभीर निहितार्थों वाली होती हैं, विशेष रूप से कृषि जैसे राज्य सूची के विषय के संदर्भ में।
अखिल भारतीय सेवाएं: अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र के विशिष्ट अधिकार क्षेत्र में हैं। कुछ शक्तियां राज्यों के साथ बांटी जा सकती हैं। राज्य सरकारों की अखिल भारतीय सेवाओं के नियमों एवम विनियमों के प्रशासन में विशिष्ट रूप से एक बड़ी भूमिका होनी चाहिए।
वित्तीय मुद्दे
भारत में राजस्व संघवाद हमेशा से बेहद समस्यात्मक रहा है। लम्बवत् एवं क्षैतिज असंतुलन ने केवल अभी तक बने हुए हैं, अपितु कई मामलों में अधिक जटिल भी हो गए हैं।
लम्बवत् असंतुलन: संघ-राज्य संबंधों के संदर्भ में भारतीय संविधान में आधारभूत असंतुलन इस तथ्य से पैदा होता है कि, जबकि विकास व्यय (सिंचाई, सड़क, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि) और प्रशासनिक व्यय (कानून व्यवस्था, सामान्य प्रशासन इत्यादि) क्षेत्रों में बड़ी जिम्मेदारियां राज्यों को दी गई हैं, राजस्व संग्रहण की बेहद महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र को दी गई है।
अपर्याप्त राजस्व वितरण: केन्द्रीय करों के राज्यों को आवंटन के एक निष्पक्ष सिद्धांत पर कार्य करने की बेहद आवश्यकता है।
करारोपण की अवशिष्ट शक्तियां: राज्य करारोपण की अवशिष्ट शक्तियों को, विशिष्ट रूप से सेवाओं पर कर, राज्य को हस्तांतरित करने की न्यायसंगत मांग करते रहे हैं। इस मांग को दरकिनार करते हुए, केंद्र ने संविधान संशोधन द्वारा सेवाओं पर कर लगाने की समस्त शक्तियां प्राप्त कर लीं।
वित्त आयोग के माध्यम से शर्तों का आरोपण: 11वां वित्त आयोग केंद्रीय राजस्व में राज्यों के हिस्से को 29.5 प्रतिशत से अधिक अनुशंसित करने या ऋण राहत देने में विफल हो गया। 12वें वित्त आयोग ने भी राज्यों पर विभिन्न शर्तों को थोपा, उनमें से एक थी कि, राज्यों को ऋण राहत और केंद्र से कर पुनर्संरचना प्राप्त करने के लिए राजस्व उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम को लागू करना होगा।
राज्य लघु बचत कोष ऋण: केंद्र के ऋण लघु बचत संग्रहण (राष्ट्रीय बचत योजना कोष) से सम्बद्ध होते हैं जिसमें विशेष भार पड़ता है क्योंकि राज्यों से संघ सरकार द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज दर बेहद ऊंची होती है अपेक्षाकृत जमाकर्ता को दी जाने वाली ब्याज दर के बराबर। राज्यों ने बारहवें वित्त आयोग को इस बारे में समाधानपरक उपाय सुझाने के लिए गुहार लगाई। हालांकि, राज्यों की किसी भी बड़ी समस्या को तवज्जो नहीं दी गई।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) से समस्या: केंद्र प्रायोजित योजनाओं में तीव्र वृद्धि, जिनका निर्माण एवं कार्यान्वयन राज्य सरकार के साथ बिना किसी पर्याप्त विचार-विमर्श के पूरी तरह से केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है, एक अन्य गंभीर समस्या है। यह बेहद केंद्रीकृत एवं कठोर रूपरेखा वाली योजनाएं प्रायः राज्यों की विशिष्ट जरूरतों से असंगत हो जाती हैं। क्योंकि अधिकतर मामलों में इन योजनाओं के व्यय पर एक हिस्सा राज्य सरकार का होता है, राज्य सरकार अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इन पर अपने संसाधनों का आवंटन करने में बेहद कठिनाई महसूस करती है। इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं के माध्यम से, शर्तों को थोपा जाता है, जो राज्यों की स्वायत्तता की निर्बंधित करती है।
संस्थागत एवं अन्य मुद्दे
संस्थागत निकाय, जिनके माध्यम से केंद्र-राज्य संबंधों से सम्बद्ध मुद्दों को विचार विमर्श एवं हल किया जाता है, वे हैं- अंतरराज्यीय परिषद्, राष्ट्रीय एकता परिषद्, राष्ट्रीय विकास परिषद्, योजना आयोग, वित्त आयोग एवं भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड एवं अन्य वित्तीय समस्याएं हैं। हालांकि, विगत परिदृश्य दिखाता है कि न तो इन निकायोंने राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ प्रभावी कार्य किया है और न ही इनके निर्णय राज्यों के प्रति निष्पक्ष थे। इनका यह दृष्टिकोण एवं व्यवस्था परिवर्तित करने की आवश्यकता है।
कई अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय मुद्दे हैं, जो केंद्र राजर संबंधों में महत्वपूर्ण हैं। इनमें बड़े सिंचाई कार्यक्रम, बड़ी नदियों का अपरदन, केन्द्रीय सार्वजानिक उपक्रमों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्गों, पत्तनों, हवाई अड्डों इत्यादि में केंद्रीय निवेश जैसे विषय शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक मुद्दे में केंद्र एवं राज्यों के हित शामिल हैं, और यह आवश्यक है की निर्णयों को लेने में अंतरराज्यीय संतुलन सुनिश्चित किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त करने, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की पहचान करने और अनिवार्य वस्तु अधिनियम का प्रशासन, जो मुद्रास्फीति की कम करने में बेहद प्रासंगिक बन गया है, जैसे मुद्दे भी हैं।
राज्यों के लिए राहत कोष में वृद्धि के चलते राष्ट्रीय आपदा राहत कोष की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। खनिज संसाधनों पर अंतरराज्यीय प्रतिस्पर्द्धा को ध्यान रखते हुए, खनिज उत्खनन के संदर्भ में कुछ साझा मूल्य एवं मापदंड निर्धारित करने की आवश्यकता है। कोयले एवं अन्य खनिजों पर रॉयल्टी दरों को बेहद तेजी से संशोधित किए जाते रहना चाहिए और एडवोलोरेम आधार पर अधिभार लगाना चाहिए। बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा साख वितरण नीतियों में राज्य सरकारों को भी शामिल किया जाना बेहद महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से प्राथमिक क्षेत्रक कर्ज के उचित आवंटन को सुनिश्चित करने एवं ऋण वितरण के क्षेत्र में अंतरराज्यीय संतुलन बनाए रखने के लिए इन मुद्दों के प्रभावी समाधान के लिए सुस्थापित संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता है जहां नियमित रूप से केंद्र-राज्य एवं अंतरराज्यीय विचार-विमर्श हो सके और निर्णयों तक पहुंचा जा सके।
केंद्र-राज्य संबंधों में सुधार
स्वतंत्रता प्राप्ति से 1967 तक संघ-राज्य संबंधों में टकराव की स्थिति नहीं थी क्योंकि अमूमन केंद्र एवं राज्य स्तर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 1967 के पश्चात् जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात् आपसी विरोध मुखर हो उठे एवं केंद्र-राज्यों के मध्य शक्ति एवं स्वायत्तता की मांग उठने लगी फलस्वरूप इस दिशा में सुधार अपरिहार्य हो गया। सुधारों को तीव्र गति देने हेतु वर्ष 1966 में एक प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया। प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों के अध्ययन एवं सुझाव हेतु एम.सी. सीतलवाड़ की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का गठन किया।
सीतलवाड़ समिति: इस समिति ने संविधान में अधिक फेरबदल किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की संस्तुति की। इसने ऐसा करने के दो उद्देश्य बताए। प्रथमतः, इससे केंद्र-राज्य में मौजूद तनाव में कमी आएगी। दूसरे, केंद्र एवं राज्यों के प्रशासन में कर्मठता आएगी।
राजमन्नार समिति: तमिलनाडु सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों के मध्य तनाव को हल करने के उद्देश्य हेतु डा. पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में एक समिति का 22 सितंबर, 1969 में गठन किया। इसने अपनी रिपोर्ट मई 1971 में तमिलनाडु सरकार को सुपुर्द की। इसकी मुख्य सिफारिशें थीं-
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सदस्यता वाली एक अंतरराज्यीय परिषद का तुरंत गठन किया जाना चाहिए।
- प्रतिरक्षा एवं वैदेशिक मामलों को छोड़कर कोई भी अन्य-विषय अंतरराज्यीय परिषद् की सहमति के बिना निर्णय नहीं किया जाना चाहिए।
- अवशिष्ट विषय को समाप्त कर दिया जाना चाहिए अन्यथा राज्यों की दिए जाने चाहिए।
- अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए।
- योजना आयोग का विघटन किया जाना चाहिए एवं इसके स्थान पर राज्यों का अपना नियोजन बोर्ड होना चाहिए।
- वित्त आयोग का गठन स्थाई आधार पर होना चाहिए।
- कुछ विषयों को संघ एवं समवर्ती सूची से हटाकर राज्य सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
इन सब समिति एवं आयोगों के पश्चात् जब 1977 में पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र को संविधान में संशोधनों की मांग के साथ राज्यों में स्वायत्तता में वृद्धि की बात कही एवं इसी समय पंजाब के अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पेश किया जिसमें केंद्र के अधिकार क्षेत्र को वैदेशिक, प्रतिरक्षा, रेलवे, मुद्रा एवं संचार तक सीमित रखने की मांग की गई, तो इन सब बातों के संदर्भ में केंद्र सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों के समग्र अवलोकन हेतु सरकारिया आयोग का गठन किया।
सरकारिया आयोग
जून 1983 में न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का गठन केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति के समान वितरण से संबंधित सुझाव देने के लिए किया गया था। इस आयोग के दो अन्य सदस्य एस.आर. सेन और बी. शिवरामन थे। इन सदस्यों के अतिरिक्त इस आयोग में एक सचिव, एक संयुक्त सचिव और चार निदेशक थे। इस आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 4,900 पृष्ठों वाली इस रिपोर्ट ने कुल 247 सिफारिशें कीं। ये सिफारिशें केंद्र और राज्यों के वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों से संबंधित हैं। इस आयोग पर कुल 150.61 लाख रुपए खर्च हुए।
सरकारिया आयोग ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की केंद्र सरकार की शक्ति को उचित ठहराया, परंतु इसके साथ ही आयोग ने चेतावनी दी है कि इस शक्ति का प्रयोग बहुत ही कम और केवल उस समय किया जाना चाहिए जब स्थायी तथा लोकतांत्रिक सरकार को कायम रखने के लिए दूसरे सभी साधन असफल हो गए हों। आयोग ने यह सिफारिश की कि, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तभी लागू किया जाना चाहिए यदि उसकी आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए ठोस तथ्य तथा सबूत हों। राज्यपाल को ऐसे सभी तथ्य उसी रिपोर्ट के साथ लगाने चाहिए, जो रिपोर्ट वह राष्ट्रपति को भेजता है। ऐसी रिपोर्ट को गुप्त नहीं रखा जाना चाहिए। आयोग ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 356 में संशोधन करके यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्यपाल की रिपोर्ट में वर्णित सभी तथ्य राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली घोषणा के भाग होने चाहिए। आयोग के अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा जारी करने से पूर्व उस राज्य की सरकार की एक चेतावनी दी जानी चाहिए। यदि सम्बद्ध सरकार चेतावनी पर ध्यान न दे तो फिर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आयोग ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश की, कि किसी राज्य की विधान सभा को संसद की स्वीकृति के पश्चात् ही भंग किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ आयोग ने यह सिफारिश भी की कि, राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने से पूर्व संबंधित राज्य सरकार से विचार-विमर्श कर लेना चाहिए।
यद्यपि आयोग ने केंद्रीय सरकार की शक्तियों को कम करने की मांग रद्द कर दी। आयोग ने यह सिफारिश की कि देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए शक्तिशाली केंद्र का होना आवश्यक है। परंतु आयोग ने संविधान के अनुच्छेद-258 (कुछ दशाओं में राज्यों की शक्ति हस्तांतरित करने संबंधी केंद्र सरकार का अधिकार) का प्रयोग केंद्र द्वारा उदारतापूर्वक किए जाने की सिफारिश की।
सरकारिया आयोग ने समवर्ती-सूची में राज्य की अधिक अधिकार प्रदान करने तथा इस सूची पर केंद्र को उदार रवैया अपनाने की सिफारिश की। आयोग ने यह भी कहा कि समवर्ती-सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने से पूर्व केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करना चाहिए।
यद्यपि आयोग ने संसद की राज्य विधानमंडल से सर्वोच्च संस्था तो माना किंतु साथ ही यह सिफारिश भी की, कि राज्य विधानमंडल को संविधान संशोधन द्वारा और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। फलस्वरूप राज्य अनुच्छेद 252 के अंतर्गत राज्य-सूची से संबंधित संसदीय कानूनों में राष्ट्रपति की सहमति से संशोधन कर सकते हैं।
आयोग ने यह सिफारिश की, कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करने से पूर्व केंद्रीय सरकार को सम्बद्ध राज्य के मुख्यमंत्री को विश्वास में लेना चाहिए। आयोग ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के साथ विचार-विमर्श की शर्तो की संविधान में व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए।
आयोग ने यह सिफारिश की कि, किसी भी न्यायाधीश का उसकी स्वीकृति के बिना किसी एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चाहिए कि वह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के संबंध में अपना परामर्श देने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों का परामर्श अवश्य लें।
आयोग ने अपनी सिफारिश में वित्त आयोग तथा योजना आयोग के मध्य परस्पर सहयोग पर बल दिया। साथ ही राजस्व के क्षेत्र में राज्य के हिस्सों को बढ़ाने का सुझाव दिया। मुख्य रूप से वित्तीय दृष्टि से कमजोर राज्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता व्यक्त की। आयोग का यह भी कहना था कि राज्यों का वित्तीय लाइसेंसिंग पर अधिकतम नियंत्रण होना चाहिए।
आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के अनुसार, सामाजिक आर्थिक नियोजन तथा विकास के लिए अंतरराज्यीय परिषद के गठन पर बल दिया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव से संबंधित राज्यों की स्वायत्तता को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया।
पुंछी आयोग
केंद्र-राज्य संबंधों की फिर से व्याख्या करने के लिए अप्रैल 2007 में एक नए आयोग का गठन किया गया। उच्चतम न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किये गये। चार सदस्यीय इस आयोग के अन्य सदस्य धीरेंद्र सिंह और वी. के. दुग्गल दोनों पूर्वगृह सचिव तथा एन.आर. माधव राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के पूर्व निदेशक थे। यह आयोग सरकारिया आयोग के गठन के दो दशक से अधिक समय बाद अस्तित्व में आया था। आयोग इस बात की संभावना तलाश करेगा कि किसी राज्य में स्वतः संज्ञान के आधार पर केंद्र सरकार केंद्रीय बलों को तैनात कर सके और देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच करा सके। इसमें कर और नदी संयोजन के मुद्दे भी शामिल हैं। आयोग यह भी तय करेगा कि सांप्रदायिक हिंसा, जातीय हिंसा या अन्य तरहके सामाजिक संघर्ष भड़कने की स्थिति में केंद्र की भूमिका जिम्मेदारी और अधिकार क्षेत्र क्या होगा?
आयोग इस बात की भी समीक्षा करेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर स्वतः संज्ञान लेकर कोई केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसी बनाई जा सकती है अथवा नहीं। सरकारिया आयोग का स्थान लेने वाले इस आयोग के कार्यक्षेत्र में अनुच्छेद-355 में नया उपबंध जोड़ने का काम भी होगा। इसके तहत जरूरत पड़ने पर राज्यों में स्वतः संज्ञान लेकर केंद्रीय बलों की तैनाती की जा सकेगी।
नया आयोग इस बात पर भी ध्यान देगा कि केंद्र और राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसी भूमिका निभाएं जो पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को ज्यादा शक्ति और स्वायत्तता प्रदान करें। आयोग के कार्यक्षेत्र में जिला स्तर पर स्वतंत्र रूप से योजना बनाने और बजट बनाने की परिकल्पना की बढ़ावा देना शामिल है। इस दिशा में 3 जनवरी, 2008 को आयोग ने विभिन्न विचारित मुद्दों पर व्यक्तियों विभिन्न संगठनों, संस्थाओं एवं समूहों से उनके विचार एवं सुझाव आमंत्रित किए। आयोग ने 5 मार्च, 2008 को 63 पृष्ठों की एक प्रारूप प्रश्नावली प्रकाशित की एवं समस्त राज्यों तथा मुख्य सरकारी कार्यालयों में, इसमें उल्लिखित प्रश्नों में से उनकी पसंद के प्रश्नों पर उनके विचार जानने के उद्देश्य से, वितरित किया। इस आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं-
- आयोग भारत के संविधान के अनुसार संघ एवं राज्यों के बीच विद्यमान व्यवस्थाओं के कार्य संचालनअपनाएं जा रहे स्वास्थ्य दृष्टान्तों, विधायी संबंधों, प्रशासनिक संबंधों सहित सभी क्षेत्रों में शक्तियों, कार्यों एवं दायित्वों के संबंध में न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों, राज्यपालों की भूमिका, आपातकालीन उपबंधों, वित्तीय संबंधों, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, पंचायती राज संस्थाओं, अंतर्राज्यीय नदी जल सहित संसाधनों के बंटवारे की जाँच और समीक्षा करेगा और व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ऐसे परिवर्तनों अथवा उपायों की सिफारिश करेगा जो उपयुक्त हों।
- केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं के कार्य सब्चालन की जांच और समीक्षा करते समय और अपेक्षित परिवर्तनों और उपायों की सिफारिशें करते समय आयोग उन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की ध्यान में रखेगा जो पिछले वर्षों, खासतौर पर पिछले दो दशकों में हुए हैं और योजना तथा संविधान के ढांचे का पूरा सम्मान करेगा। ऐसी सिफारिशें आवश्यक होगी जिनसे देश की एकता और अखण्डता को सुदृढ़ करते हुए लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सुशासन सुनिश्चित करने की नई चुनौतियों से निपटा जा सके और नई सहस्राब्दि के प्रारम्भिक दशकों में गरीबी और अशिक्षा के उन्मूलन के लिए सतत् तथा तीव्र आर्थिक विकास के नए अवसर प्राप्त किए जा सकें।
- उपर्युक्त के संबंध में जांच और सिफारिशें करते समय आयोग द्वारा निम्नलिखित का विशेष ध्यान रखा जाएगा किंतु वह अपने अधिदेश को इन तक ही सीमित नहीं रखेगा-
- सांप्रदायिक हिंसा, जातीय हिंसा के बड़े पैमाने पर एवं दीर्घकाल तक जारी रहने के दौरान अथवा अन्य किसी सामाजिक संघर्ष, जिसके फलस्वरूप दीर्घकालिक एवं तीव्र हिंसा हुई हो, के दौरान राज्यों की तुलना में में केंद्र की भूमिका, उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार।
- बड़ी परियोजनाओं की योजना तथा कार्यान्वयन में राज्यों की तुलना में केंद्र की भूमिका, उत्तरदायित्व एवं क्षेत्राधिकार जैसे कि नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना जिन्हें पूरा होने में आमतौर पर 15-20 वर्ष लगेंगे और ये पूरी तरह राज्यों के समर्थन पर निर्भर हैं।
- संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त निकायों सहित शक्तियों एवं स्वायत्तता के प्रभावी प्रत्यायोजन को बढ़ावा देने में राज्यों की तुलना में केंद्र की भूमिका, उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार।
- जिला स्तर पर स्वतंत्र नियोजन एवं बजट बनाए जाने की अवधारणा और प्रथा को बढ़ावा देने में राज्यों की तुलना में केंद्र की भूमिका, उत्तरदायित्व एवं क्षेत्राधिकार।
- विभिन्न प्रकार की केंद्रीय सहायता की राज्यों की भूमिका के साथ सम्बद्ध करने में राज्यों की तुलना में केंद्र की भूमिका, उत्तरदायित्व एवं क्षेत्राधिकार।
- विशेष रूप से केंद्र से निधियों के अंतरण पर राज्यों की अधिक निर्भरता को देखते हुए केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में 8वें से 12वें वित्त आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों का प्रभाव।
- मूल्य संवद्धित कर प्रणाली की शुरुआत होने के पश्चात् माल के उत्पादन में बिक्री पर अलग-अलग कर लगाए जाने की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता।
- पिछड़े राज्यों के पक्ष में सकारात्मक विभेद के आधार पर दृष्टिकोण तथा नीतियों को अंगीकार कराने में केंद्र की भूमिका, उत्तरदायित्व एवं क्षेत्राधिकार।
- एक एकीकृत एवं अखण्डित घरेलू बाजार स्थापित कराने के उद्देश्य से तथा सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के अध्याय xviii में दी गई इसकी सिफारिशों को स्वीकार करने में राज्य सरकारों की अनिच्छा के संदर्भ में भी अंतरराज्यीय व्यापार को मुक्त करने की आवश्यकता।
- एक ऐसी केंद्रीय विधि प्रवर्तन एजेंसी स्थापित किए जाने की आवश्यकता जो उन अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत हो जिनकी अंतरराज्य तथा अंतरराज्यीय व्याप्ति हो एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ते हों।
- राज्यों में केंद्रीय बलों की, जब और जहां परिस्थितियों की ऐसी मांग हो, स्वतः तैनाती के उद्देश्य से अनुच्छेद-355 के अंतर्गत एक समर्थ विधायन की व्यवहार्यता।
पुंछी आयोग रिपोर्ट की अनुशताएं
- भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश एम. पुंछी की अध्यक्षता में गठित केंद्र-राज्य संबंध आयोग ने सरकार को 20 अप्रैल, 2010 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें अनुच्छेद-355 और अनुच्छेद-356 के राज्य सरकारों को बर्खास्त करने में दुरुपयोग को रोकने के लिए रोकथाम उपाय प्रस्तावित किए हैं।
- अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 को लेकर जो भी प्रश्न उठे हैं, उन सबका इस रिपोर्ट में उत्तर दिया गया है, ऐसा आयोग के अध्यक्ष का कहना है।
- आयोग ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) जैसे नवगठित संस्थान का भी अध्ययन किया है और एनआईए को सौंपे गए आतंकी जांचों में राज्यों के निर्बाध सहयोग को सुनिश्चित करने की प्रक्रियाओं की अनुशंसा भी की है।
- रिपोर्ट के सात भाग हैं, जिसमें पहला केंद्र-राज्य संबंधों के उद्गम की चर्चा करता है। दूसरा भाग इनके संवैधानिक योजनाओं की तरफ जाता है जिसमें अनुच्छेद-19, 355, 356 और 263 से संबंधित अनुशंसाएं भी शामिल की गई हैं।
- तीसरे भाग में आर्थिक और वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है और इसमें प्रादेशिक असंतुलनों को दूर करने के नियोजन मॉडल के उन्नयन की अनुशंसा शामिल की गई है।
- चौथा भाग 73वें एवं 74वें संशोधन एवं छठी अनुसूची से सम्बद्ध अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है।
- पंचाव भाग आतंरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नस्लवाद, घुसपैठ एवं सांप्रदायिक हिंसा जैसे विषयों को विशेष रूप से शामिल करता है।
- छठा भाग पर्यावरण मुद्दों एवं संसाधन हिस्सेदारी, विशेष रूप से नदियों एवं खनिजों, की बात करता है।
- सातवां भाग सामाजिक विकास एवं सु–शासन के मामले को शामिल करता है।
संघ-राज्य आयोग का उद्देश्य संघीय ढांचे के निर्बाध कार्यकरण को सुनिश्चित करना रहा है।
आंतरिक सुरक्षा एवं केंद्र-राज्य संबंध
राष्ट्रीय सुरक्षा की आंतरिक चुनौतियां भारतीय सुरक्षा पर चर्चा का मुख्य केंद्र माना गया है। इस पर बहस है कि बाह्य खतरों की तुलना में यह बेहद गंभीर चुनौती है। इसकी उपस्थिति पूरे भारत के समानांतर है और इसे भारत के उत्तर एवं उत्तर-पूर्व सीमा तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसलिए इस खतरे से निपटने की चिंता केंद्र एवं राज्यों दोनों के लिए समान है। हालांकि, यह जाहिर है कि चाहे मुम्बई हमलों से निपटने की बात हो, या जम्मू एवं कश्मीर में उपद्रव का मामला हो, या मणिपुर में एनएससीएन (आईएम) द्वारा चक्का जाम करने की घटना ही, या नक्सल क्षेत्रों में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस के बीच समन्वय के अभाव का मामला हो, भारतीय राजव्यवस्था की संघीय प्रकृति केंद्र एवं सम्बद्ध राज्यों के बीच तनाव उत्पन्न करती है।
विभिन्न आतंकवादी हमलों की पृष्ठभूमि से यह मांग उठती रही है कि भारत में ऐसी सशक्त संस्था हो जो आंतरिक सुरक्षा की चुनौती से निपट सकें। आतंकवादी हमलों को राज्यों की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी मानकर केंद्र सरकार की संघीय परिदृश्य में निष्क्रिय भूमिका नहीं निभानी चाहिए। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आतंकवादी निरोधक केंद्र (एनसीटीसी) की स्थापना का मसौदा तैयार किया। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ओडीशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तथा अन्यों ने इसका प्रबल विरोध किया। यह राज्यों से विचार-विमर्श न करने का ही दुष्परिणाम है कि ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या आतंकवाद निरोधक केंद्र की राज्य सरकारों की मंजूरी बिना भी उनके यहां हर तरह की कार्रवाई का अधिकार होगा?
राज्यों का मानना है की आतंकवाद का सम्बन्ध सिर्फ केंद्र सरकार से नहीं है अपितु देश के सभी राज्य इससे प्रभावित हैं। ऐसे में आतंकवाद से संबंधित किसी भी निर्णय में राज्यों से सलाह मशविरा करना जरूरी है और केंद्र सरकार द्वारा इस बात की अनदेखी की गई है। विरोधियों का यह भी मानना है कि एनसीटीसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत कार्य करेगी जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार अपने राजनितिक विरोधियों के लिए करती आई है। अतः एनसीटीसी का इस्तेमाल केंद्र सरकार वैसे राज्यों के विरोध में कर सकती है जो विरोधी राजनीतिक दल द्वारा शासित है। अतः एनसीटीसी का उपयोग ऐसे राज्यों के विरोध के एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। राज्यों का मानना है कि एनसीटीसी संविधान में दी गई संघीय परम्परा के प्रतिकूल है।
वास्तव में आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर कोई भी निर्णय लेते समय राज्यों के साथ विचार-विमर्श आवश्यक है जिसकी अनदेखी की गई है। देश की संघीय व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आवश्यक है की केंद्र द्वारा राज्य प्रतिनिधियों के साथ विमर्श कर इस समस्या को सुलझाया जाय।
संवैधानिक प्रावधान
संविधान के अनुच्छेद-11 में केंद्र और राज्यों की विधायी और प्रशासनिक शक्तियों को स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा यदि संविधान के 245-261 तक के अनुच्छेदों की अनुच्छेद-355 के साथ पढ़ा जाए, जो कहता है कि यह केंद्र का दायित्व है कि वह बाहरी हमलों और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करे, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य, दोनों ही सरकारों की है। सभी मानते हैं कि आतंकवाद एक राष्ट्रीय चुनौती बन चुका है सभी इस बात पर भी एकमत हैं कि देश की एकता एवं अखंडता को चुनौती वाली ताकतों से लोहा लेने की जरूरत है। सभी दलों के प्रतिनिधि संसद में आतंकवाद विरोधी अधिनियमों पर अपनी सहमति जता चुके हैं। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट (पोटा) और अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट इसकी मिसाल हैं।
भारत जैसे विशाल देश में आंचलिक क्षेत्रों में अलगाव की प्रवृति अस्वाभाविक नहीं है। पूर्वोत्तर, पंजाब और कश्मीर के आतंकवादी गुटों से लैस संगठित तंत्र के रूप में आज आतंकवाद भारत संघ के सामने बड़ी चुनौती बन गया है। यह तो कोई भी स्वीकार करेगा कि कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय है, लेकिन आतंकवाद खासकर वैश्विक जेहादी समूहों का जो व्यापक तंत्र चारों ओर फैल चुका है उसका मुकाबला केवल राज्य नहीं कर सकते। इसलिए एक ऐसी शीर्ष राष्ट्रीय एजेंसी अपरिहार्य है, जो देश भर में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को समन्वित करे तथा उसकी दिशा पर एकरूपता का निर्धारण करे, जिस एक प्रावधान पर इन राज्यों की सर्वाधिक आपत्ति है वह है इसकी गुप्तचर एजेंसी को दिया गया छानबीन एवं गिरफ्तारी का अधिकार। इसके बाद आतंकवाद के किसी मामले में केंद्रीय एजेंसियों को कहीं भी किसी की तलाशी लेने का अधिकार होगा और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर वह किसी को गिरफ्तार कर सकती है। इसमें राज्यों की पुलिस की तो विश्वास में लिया जा सकता है, लेकिन उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह गुप्तचर ब्यूरो का भाग बना दिए जाने के कारण यह आशंका भी पैदा हो रही है कि भविष्य में केंद्र सरकारें इसका दुरुपयोग कर सकती हैं। इन सब समस्याओं के बीच आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि वर्तमान आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के मद्देनजर हम संघीय ढांचे को किस प्रकार सुरक्षित रख पाते हैं?
संघ-राज्य सम्बन्धों में सुधार हेतु सुझाव
- अंतरराज्यीय संबंधों के संदर्भ में संघ सरकार द्वारा अधिक हस्तक्षेप किए जाने के स्थान पर अंतरराज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद इत्यादि की प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए।
- वित्त आयोग की नियुक्ति एवं उसे अतिरिक्त विषय प्रदान करने के सम्बन्ध में राज्यों से उपयुक्त परामर्श किया जाना चाहिए।
- संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के सम्बन्ध में वित्त आयोग की सिफारिशें और बेहतर एवं प्रभावी बनाई जानी चाहिए।
- अनुच्छेद-356 का संघ द्वारा दुरुपयोग करने पर कुछ अंकुश लगाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में राज्यपाल के प्रतिवेदन को उपयुक्त रूप से ध्यानागत तो रखा जाना चाहिए किंतु उससे पूर्व राज्यपाल के पद एवं कार्यों की प्रवृत्ति में यथोचित सुधार लाए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद-356 लगाए जाने के पूर्वसम्बन्धित राज्यों को चेतावनी दी जानी चाहिए।
- प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रेषित एक सुझाव एवं नौवीं पंचवर्षीय योजना में व्यक्त एक मत के अनुसार, संघ द्वारा नियोजित कार्यक्रमों को कुछ स्थितियों, जैसे- अंतर्राज्यीय समन्वय की आवश्यकता, राज्य तंत्र के पास आवश्यक क्षमता न होने, क्षेत्रीय असमानताओं की कम करने हेतु आवश्यक स्थितियां, आदि,तक सीमित रखा जाना चाहिए।
- राज्यपाल की नियुक्ति के समय सम्बन्धित राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त त्रिशंकुविधानसभा की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में बेहतर दिशा-निर्देश, सक्रिय राजनीतिज्ञ को राज्यपाल नियुक्त न करने, विश्वास प्रस्ताव हेतु समय देने के सम्बन्ध में न्यूनतम और अधिकतम समय के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश प्रेषित किए जाने चाहिए।
- सरकारिया आयोग के मतानुसार, संघ-राज्य सम्बन्धों को और बेहतर एवं सुदृढ़ बनाने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद को पर्याप्त रूप से प्रभावी बनाते हुए नियोजन के सम्बन्ध में इसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक समन्वय को प्राप्त किया जाना चाहिए।
- अखिल भारतीय सेवाओं से सम्बन्धित प्रतिनियुक्तियों, विषयों, सेवा विस्तार, इत्यादि के सम्बन्ध में एक निष्पक्ष एवं व्यावसायिक संस्था के माध्यम से अथवा उसके परामर्शानुसार निर्णय लिए जाने चाहिए।
- राज्यों पर पर्याप्त प्रभाव डालने वाले संवैधानिक संशोधनों के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य/राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए।
- नियोजन से संबंधित राज्य विकास परिषद के मतों की राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नियोजन सम्बन्धी दिशा-निर्देश बेहतर एवं स्पष्ट होने चाहिए ताकि राज्य नियोजन तंत्र एवं राष्ट्रीय नियोजन तंत्र, दोनों ही इन विषयों को बेहतर ढंग से ध्यान में रख सकें।
- कुछ परिस्थितियों में संघ सरकार के अधिक हस्तक्षेप के स्थान पर कुछ स्वायत्त संस्थाओं को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, मानवाधिकार हनन सम्बन्धी विषयों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, इत्यादि को पर्याप्त अधिकार प्रदान करके प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
- राज्य के विधानमण्डल में अथवा समिति व्यवस्था में राज्य की विधायी शक्ति के संबंध में बेहतर जानकारी एवं विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि विधायी प्रक्रिया में सम्बन्धित विधेयकों में इस प्रकार के सुधार लाए जा सकें, जिनसे उन्हें आरक्षित करने की आवश्यकता न पड़े।
- राज्यों की व्यय एवं ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु उनके व्यय एवं ऋण का मूल्यांकन अनुभवी विशेषज्ञों तथा निष्पक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से वस्तुस्थितियों की जानकारी रखने वाली संस्थाओं के द्वारा किया जाना चाहिए तथा इन ऋणों एवं नुदानों को राज्य की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
राष्ट्रीय एकीकरण (राष्ट्र निर्माण) की चुनौतियां एवं समाधान
भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है- यहां क्षेत्रीय विविधता, धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक विविधता, जातिगत विविधता और भाषागत विविधता यत्र-तत्र दिखाई देती है। जिस देश में इतनी अधिक विविधताएं हों, वहां एकता की स्थापना और उसे कायम रखना बहुत ही मुश्किल होता है। भारत में विविधताओं को कायम रखते हुए ही एकीकरण की दिशा में प्रयत्न करना आवश्यक है।
वस्तुतः, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना की नीव 1905 के बंग-भंग के विरोधस्वरूप शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन में ही पड़ी, किन्तु वास्तविक एकता का प्रमाण राष्ट्रीय आंदोलन में मोहनदास करमचंद गांधी के आने के बाद ही दृष्टिगत होता है। गांधीजी के आगमन से पूर्व स्वतंत्रता आंदोलन शहरी एवं शिक्षित उच्च वर्ग तथा मध्यम वर्ग तक ही सीमित था, किन्तु उनके आगमन के बाद ग्रामीण अशिक्षित निम्न वर्ग ने भी आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लेना शुरू कर दिया। 1920 के दशक से तो ऐसा लगने लगा जैसे अब भारतीयों की एकजुटता देखकर अंग्रेज जल्दी ही देश छोड़ देंगे। किन्तु, विविधता ने स्वतंत्रता आंदोलन को भी प्रभावित किया- कुछ गुट उदारवादी थे, तो कुछ उग्रवादी, कुछ दल साम्प्रदायिकता की भावना से भी प्रेरित थे। इसका परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को दो भागों में बांट दिया गया- हिन्दुस्तान (भारत) और पाकिस्तान के रूप में। बाद में पाकिस्तान का भी विभाजन हो गया (1971 में) और बांग्लादेश के नाम से एक नया देश बना।
राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ यह कदापि नहीं है कि विविधताओं का अंत कर सम्पूर्ण देश में एक धर्म या एक भाषा को अपनाने पर मजबूर कर दिया जाए। भारत के राष्ट्रीय एकीकरण से तात्पर्य है विविधताओं को कायम रखते हुए देश की एकता और अखण्डता को सुरक्षित रखना। दूसरे शब्दों में, व्यक्तिगत हितों एवं राष्ट्रीय हित के बीच समन्वयात्मक सामंजस्य की स्थापना राष्ट्रीय एकीकरण है। राष्ट्रीय एकीकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए इस अवधारणा का विकास नितांत आवश्यक है की व्यक्तिगत, समूहगत, सम्प्रदायगत अथवा भाषागत सभी हितों से ऊपर राष्ट्रहित है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत द्वारा नए संविधान का निर्माण किया गया और देश के सभी नागरिकों को विकास का समान अवसर प्रदान करने के लिए उनमें से किसी के भी साथ धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र अथवा लिंग-भेद के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार को गैर-कानूनी घोषित किया गया। इसके साथ ही, देश में शासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई और इसके द्वारा स्वतंत्रता तथा समानता की स्थापना पर बल दिया जाने लगा। संविधान की प्रस्तावना में तो धर्म-निरपेक्षता (पंथ निरपेक्षता) की घोषणा कर दी गई, परन्तु स्वतंत्रता और समानता की आड़ में भारत में साम्प्रदायिकता और जातीयता की भावना के साथ-साथ क्षेत्रीयता और भाषागत भावनाएं भी बढ़ गई। इन सब ने मिलकर देश की एकता और अखण्डता की सुरक्षा के लिए ही खतरा उत्पन्न कर दिया।
जातीयता
भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सर्वाधिक प्राचीन समस्या जातीयता है। उत्तर वैदिक काल में जाति-विभाजन की जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसने गुप्त काल में आकर इतनी जटिलता ग्रहण कर ली कि इस समस्या से मुक्ति पाना आज भी मुश्किल ही नहीं असंभव भी प्रतीत होता है। विभिन्न प्रकार की छोटी-बड़ी जातियों ने समाज को छोटे-छोटे समूहों में बांट दिया है और ये छोटे-छोटे समूह अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं- इस क्रम में उन्होंने राष्ट्रीय हितों की भी अनदेखी शुरू कर दी है। यह एक विडम्बना ही है कि स्वतंत्रता प्राप्ति की 60वीं वर्षगांठ मनाए जाने के बावजूद भारत में ऊंच और नीच का भेद समाप्त नहीं हुआ है- अभी भी शहरी उपभोक्ता वर्ग अपने आपको श्रेष्ठ समझता है और ग्रामीण उत्पादक वर्ग को निम्न। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अंग्रेजों की जो गोरे और काले की रंग-भेद की नीति थी, वह परिवर्तित रूप में आज भी तो विद्यमान ही है। ऐसी परिस्थिति में जातीय संघर्ष का बना रहना निश्चित है और जब तक यह संघर्ष जारी रहेगा, तब तक राष्ट्रीय एकीकरण के लिए समस्या बनी ही रहेगी।
विश्व का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है, जहां राजनीति जातिवाद से अछूती है। हां, जातिवाद का स्वरूप सभी जगह अलग-अलग है। विकसित देशों में मतदाता के शिक्षित होने के कारण जातिवाद का हिंसक एवं वीभत्स रूप प्रकट नहीं होता। परन्तु, भारत में और विशेषकर उत्तर भारत में तो जातिवाद का स्वरूप अत्यंत विकृत है। ऐसा होना भी अस्वाभाविक नहीं है। इस क्षेत्र में प्राचीन काल से ही सवर्णो द्वारा पिछड़ों का शोषण किया जाता रहा है और उन्हें किसी भी दृष्टि से ऊपर उठने से वंचित रखा गया है। इसलिए, इन राज्यों में राजनीति में जातिवाद आक्रोश के रूप में उभरा है और जब पिछड़े तबके के लोगों की राजनीति में पर्याप्त सहभागिता हो जाएगी, तब इनका आक्रोश भी कम होगा और जातीय क्रांति भी स्थिर हो जाएगी।
भारत में राजनीति में जातिवाद की विद्यमानता के लाभ भी हैं और हानि भी। जातिवाद के समावेश से लाभ निम्न वर्ण के लोगों को हुआ है, वे अब उच्च वर्ण के लोगों के समकक्ष खुद को स्थापित करने की चेष्टा करने लगे हैं, क्योंकि राजनीतिक सत्ता में उनका प्रतिनिधि भी है। और वे उसके माध्यम से अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। परन्तु दूसरी ओर जातिवाद के विकास से देश का विकास अवरुद्ध हुआ है, जातिवाद के वर्चस्व के कारण योग्य, कुशल एवं कार्यशील नेतृत्व का अभाव हो गया है। सम्पूर्ण देश में हिंसक आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया है।
सांप्रदायिकता
भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में सर्वाधिक जटिल समस्या है- साम्प्रदायिकता। 7वीं सदी के बाद भारत में मुगलों के आगमन के बाद से अब तक भारत में मुख्य रूप से दो सम्प्रदायों, हिन्दू एवं मुस्लिम, के बीच ही मुख्य रूप से प्रतिद्वंद्विता रही है। भारत में जब भी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय की बात होती है, तब अप्रत्यक्ष रूप से यह संबोधन हिन्दू एवं मुस्लिम समुदायों के लिए ही होता है। बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पर क्षेत्रीय निष्ठा का आरोप लगाते हैं, जबकि अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों पर सत्ता एवं शक्ति के दबाव का। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी मुस्लिम लीग जैसी संस्थाओं ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को विकसित किया, जबकि हिन्दू महासभा जैसी संस्थाओं ने हिन्दू साम्प्रदायिकता को। वैसे भी, भारत में मुस्लिमों का आगमन विदेशों से हुआ है और अभी तक यहां के मूल रूप में निवास करने वाले हिन्दू उनके साथ समरसता स्थापित नहीं कर पाए हैं-दोनों के रहन-सहन की पद्धति, रीति-रिवाज और खान-पान में पर्याप्त अंतर है। आरंभिक काल में जिस प्रकार मुस्लिम आक्रांताओं ने भारतीयों को जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया, उससे बहुसंख्यक भारतीयों में नफरत की भावना फैली हुई है। यह भावना शायद आठ सौ वर्षों की अवधि में समाप्त हो गई होती, परन्तु यहां के राजनेताओं ने वोट की राजनीति में अपना मतदाता वर्ग सुरक्षित रखने के लिए ऐसा नहीं होने दिया, बल्कि दोनों समुदायों को एक-दूसरे के खिलाफ लड़ाने के लिए नए-नए तरीके प्रस्तुत करते रहे।
मन्दिर-मस्जिद,पृथक् विवाह कानून आदि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिनके कारण दोनों सम्प्रदायों के बीच संघर्ष जारी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तो हिन्दू-मुस्लिम-साम्प्रदायिकता विरासत के रूप में मिली थी, किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दो राज्यों- पंजाब और नागालैंड ने सिख-साम्प्रदायिकता और ईसाई-साम्प्रदायिकता को भी उपस्थित कर दिया। नागालैण्ड में ईसाइयों एवं हिन्दू नागाओं के बीच घोर संघर्ष चल रहा है। पंजाब में विगत दो दशकों में खालिस्तान (एक पृथक् राष्ट्र) की मांग को लेकर जिस प्रकार हिंसक आंदोलन चलाया गया, उससे एक समय तो ऐसा भय लगने लगा था कि कहीं एक बार फिर भारत का विभाजन न हो जाए।
भारत में साम्प्रदायिकता के साथ-साथ उप-साम्प्रदायिकता भी है- हिन्दुओं में आर्य (सवर्ण) और अनार्य (निम्नवर्ण), मुसलमानों में शिया और सुन्नी, सिखों में अकाली और निरंकारी तथा ईसाइयों में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेण्टों के बीच भी प्रतिद्वंद्विता है। 1992 में अयोध्या (उत्तर प्रदेश)में राममंदिर और बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद जिस प्रकार से दंगे हुए, उससे भारत-विभाजन के बाद साम्प्रदायिकता का सर्वाधिक वीभत्स रूप प्रस्तुत हुआ। 2002 में गुजरात के गोधरा में हिंदू-मुस्लिम दंगों ने भारतीय धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र एवं समाज को कलंकित किया। इसके बादएक बार फिर-से भारतीय समाज में वैमनस्यता की कटु भावना व्याप्त हो गई।
भाषा
स्वतंत्र भारत में भाषावाद भी एक समस्या के रूप में उपस्थित हुआ है। हमारे देश में प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी पर ही भाषा में परिवर्तन के लक्षण दृष्टिगत होते हैं। यहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं और इनमें से अनेक भाषाओं की तो अपनी स्वतंत्र लिपियां भी हैं। भाषायी विविधता देश के विभिन्न भाषायी समूहों के बीच टकराव उत्पन्न करती है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण देश के लिए किसी एक भाषा को सर्वमान्य राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में उपस्थित नहीं कर पाना है। दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषा का वर्चस्व है, तो उत्तर भारत में भारोपीय परिवार की भाषा का\ हमारे यहाँ दक्षिण भारतीयों द्वारा तो हिंदी का विरोध किया ही जाता है, बांग्लाभाषियों तथा उर्दुभाशियों द्वारा भी इसका पर्याप्त विरोध होता है, जबकि हिन्दी भाषा-भाषियों की संख्या सर्वाधिक (लगभग 46. प्रतिशत) होने के कारण हिन्दी भाषी लोग किसी अन्य भाषा के द्वारा एकीकरण के लिए सहमत नहीं होते। हमारे देश का यह दुर्भाग्य ही है किगुलामी की प्रतीक अंग्रेजी भाषा ही आज भी प्रमुख राजभाषा के रूप स्थापित है।
भाषा सम्बन्धी मांग का एक अन्य पक्ष यह भी है की हर कोई अपनी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करवाना चाहता है। स्पष्ट है कि इस प्रकार सम्मिलित कर लेने से कोई लाभ नहीं होता है। इससे सुसंगत संविधानके दो ही उपबंध हैं- अनुच्छेद-344 (क) एवं 351। अनुच्छेद-344(क) के अनुसार, आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा के लोगों की राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है और अनुच्छेद-351 के अनुसार,उस भाषा की हिंदी भाषा के विकास में अपना योगदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। किसी भी भाषा को इस प्रकार सम्मिलित कराने के पीछे वास्तविक मंतव्य राजनीतिक होता है अर्थात् उस भाषा को बोलने वाले लोगों के लिए एक पृथक राजनीतिक इकाई की मांग, जैसे-गोरखालैण्ड अथवा बोडोलैण्ड के मामले में।
भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसे में प्रत्येक भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कराने सम्बन्धी मांग पूर्णतः निरर्थक एवं अव्यावहारिक है। अतः सरकार को चाहिए कि वह किसी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने सम्बन्धी मानकों का निर्धारण करे। सरकार द्वारा ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दुर्भाग्यवश संविधान में ऐसे किसी मानक का उल्लेख नहीं किया गया है। यही कारण है कि विभिन्न गुट इसकी मांग करते हैं, जिसे स्वीकार करने पर संघ के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न होता चला जाता है। अनेक लोगों के विचार में जो भाषाएं एक लाख से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं, आठवीं अनुसूची में शामिल कर ली जानी चाहिए। किंतु, यह विचार भी इतना असमर्थ है कि किसी भी गुट की मांग को इस विचार के आधार पर रोक पाना काफी दुष्कर है। धीरे-धीरे ये मांगें इतनी अधिक बलवती हो जाती हैं कि वे सरकार को भयाक्रांत कर देती हैं। अतः इस संदर्भ में संविधान के अंतर्गत किसी मानक को समाहित कर लेना ही उचित होगा ताकि इन पृथक्तावादी शक्तियों के विरुद्ध लड़ाई में सरकार के हाथ सशक्त हों।
अजीब बात है की घीसिंग को नेपाली भाषा के अंतर्गत आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने पर भी जनता को संतोष नहीं हुआ है। उनका कहना है कि गोरखाली को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योंकि वह गोरखा लोगों की भाषा हैजबकि नेपाली गोरखाओं को छोड़कर समस्त नेपालियों की भाषा है। इसके अतिरिक्त विगत कुछ वर्षों के दौरान आल इण्डिया उर्दू मोर्चा (All India Urdu Morcha) नामक नई पार्टी का गठन हुआ है। इसके घोषणा-पत्र में यह कहा गया है कि यदि ये जीत कर आए तो उर्दू को दूसरी राजभाषा बना देंगे। उर्दू को आठवीं अनुसूची में स्थान देना इनके लिए अपर्याप्त है। इससे ज्ञात होता है कि विभाजक शक्ति के रूप में भाषाई आंदोलन को कितना अधिक राजनीतिक महत्व प्राप्त है।
क्षेत्रवाद
1960 के दशक से भारत में क्षेत्रीयता की भावना का विकास भी राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में एक बड़ी बाधा के रूप में उपस्थित हुआ है। 1956 में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद लगभग प्रत्येक भाग में नए राज्यों की स्थापना की मांग उठायी जा रही है- पूर्वी भारत में गोरखालैण्ड (पश्चिम बंगाल का पर्वतीय क्षेत्र), बोडोलैण्ड (असम का पर्वतीय क्षेत्र) आदि राज्यों की मांग इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। केंद्र सरकार द्वारा अरुंचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड गोवा आदि राज्यों की स्थापना के बाद पृथक आन्दोलनों को अपनी मांगों को अधिक सशक्त बनाने का मौका मिला है।
क्षेत्रीयता की भावना के विकास से लाभकारी परिणाम भी मिल सकते हैं, परन्तु वर्तमान भारत में क्षेत्रीयता का जो स्वरूप उभरा है, वह हानिकारक है। 1980 के दशक के बाद से भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय शक्तियां प्रभावी भूमिका निभाने लगी हैं, जिससे राष्ट्रीय हित अंधकार की ओर बढ़ता जा रहा है। अब केंद्रीय सत्ता में क्षेत्रीय शक्तियों के दबाव में ही कार्य-संचालन होता है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर कई समस्याएं पृष्ठभूमि में चली जाती हैं और क्षेत्रीय समस्याएं प्रमुखता प्राप्त कर लेती हैं। दक्षिण भारत में तो बहुत पहले से ही क्षेत्रीय शक्तियां प्रभावी थीं, किन्तु अब उत्तर और पूर्वी भारत में भी इनका वर्चस्व स्थापित हो गया है। आज जिस प्रकार राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन के लिए झुकना पद रहा है, वह इस स्थिति को स्पष्ट कर देता है। क्षेत्रीयता के विकास के कारण केंद्रीय राजनीति अस्थिर हो गई है और प्रत्येक क्षेत्रीय समूह द्वारा व्यक्तिगत हितों को प्रमुखता दिए जाने के कारण राष्ट्रीय हितों की अनदेखी हो रही है।
शिव सैनिकों द्वारा जिस प्रकार महाराष्ट्र मराठियों के लिए नारा बुलन्द किया गया और दूसरे राज्यों के लोगों को राज्य से निकालने की धमकी दी गई तथा असोम गणपरिषद द्वारा असोम माता पहले, भारत माता बाद में का नारा बुलन्द किया गया, उससे तो यही प्रतीत होता है कि आज राष्ट्रीय हितों की खुलेआम उपेक्षा की जा रही है।
राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता पर क्षेत्रीय समूहों द्वारा डाले जाने वाले प्रभाव को कई राजनितिक चरों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे- क्षेत्रीय समूहों की संरचना एवं विचार धारा, इनके नेतृत्व की गुणवत्ता, इनकी कार्यपद्धति तथा राज्य की प्रतिक्रिया आदि।
राजनीतिक व्यवस्था को भंग करने वाले क्षेत्रीय समूहों की पहचान के लिए इनका वर्गीकरण आवश्यक हो जाता है। भारत में निम्नलिखित तीन प्रकार के क्षेत्रीय समूहों का अस्तित्व रहा है-
- वर्षों से कांग्रेस असंतुष्टों द्वारा कई क्षेत्रीय समूहों या दलों का निर्माण किया जाता रहा है। ये अल्पकालिक समूह या दल प्रायः तदर्थ आधार पर, सौदेबाजी करने के उद्देश्य से, गठित किये जाते हैं। केरल कांग्रेस, उत्कल कांग्रेस, तेलंगाना प्रजा समिति, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस आदि ऐसे दलों के उदाहरण हैं। ऐसे समूह राजनीतिक व्यवस्था में कोई गड़बड़ी पैदा नहीं करते हैं।
- जनजातीय दल दूसरे प्रकार के समूह हैं, जो किसी जनजाति विशेष की राजनीतिक पहचान बनाने तथा केंद्र से अधिकतम रियायतें हासिल करने के उद्देश्य से गठित किये जाते हैं। ये प्रायः भारत से अलग होने या पूर्णस्वतंत्रता की मांग करते हैं। नागा नेशनल काउंसिल, मिजोरम नेशनल फ्रंट, कुकी नेशनल असेम्बली जैसे उग्र समूह जनजातीय दलों के उदाहरण हैं।
- तीसरे प्रकार के क्षेत्रीय समूह वे हैं, जो प्रजातीय, सांस्कृतिक एवं भाषायी आधार पर परिभाषित क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, पंजाब, झारखंड आदि) में व्यापक जनाधार रखते हैं। तेलुगूदेशम, असम गणपरिषद, अकाली दल,द्रमुक व अन्नाद्रमुक तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा आदि इसी प्रकार के क्षेत्रीय दल या समूह हैं। ये दल सुसंगठित, व्यापक तथा भारत में बहुदलीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग के रूप अपनी भूमिका निभाने के संदर्भ में अधिक स्थिर होते हैं। राज्य विधान सभाओं में प्राप्त चुनावी बहुमत तथा संसद में अपनी उपस्थिति के कारण ये समूह गठबंधन सहयोगी या सत्तारूढ़ दल एवं विपक्षी दल के मध्य संतुलन कारक के रूप में अपनी क्रांतिक भूमिका निभाने में समर्थ होते हैं।
भारत में क्षेत्रीयता की उभरती नवीन प्रवृत्ति, विशेष रूप से आठवें दशक के उत्तरार्द्ध एवं नवें दशक की आर्थिक एवं राजनीतिक संकीर्णता की उपज है। इस दृष्टिकोण की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि भारत में अपनी पहचान के लिए सर्वाधिक बड़ा संकट असम के सामने रहा है। विदित है कि लम्बे समय तक यहां बांग्ला भाषी लोगों का प्रभाव रहा एवं नब्वे के दशक में यहां सर्वाधिक बांग्लादेशियों की घुसपैठ हुई। असमी भाषियों की चिंता निर्मूल नहीं थी कि कुछ समय बाद वे अपने ही राज्य में अल्पंसंख्यक हो जाएंगे। त्रिपुरा में भी बांग्लाभाषियों की बहुलता हो गयी है। जनगणना एवं क्षेत्रीय असंतुलन से उत्पन्न ऐसी समस्याएं देश के अन्य भागों में भी होती रही हैं। महाराष्ट्र में भी दक्षिण भारतीयों के विरुद्ध आन्दोलन संगठित हुआ एवं उत्तर भारतीयों के खिलाफ मोर्चा बन रहा है। जनसंख्या के आगमन से यह बात सिद्ध होती है कि राज्यों ने अपने यहां कुछ प्रतिबंध लागू किए हैं। उदाहरणार्थ जम्मू कश्मीर में प्रांत से बाहर के व्यक्ति को न तो वहां की नागरिकता मिल सकती है और न ही वह वहां अचल संपत्ति खरीद सकता है। हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनजातियों के हितों के लिए इन क्षेत्रों में बसने व संपत्ति खरीदने पर कुछ प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं।
भारत में क्षेत्रीयता के विकराल होते स्वरूप के सामाजिक, आर्थिक गैर-संवैधानिक संस्थाओं-वित्त आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद एवं क्षेत्रीय परिषदों ने क्षेत्रीय भावनाओं के स्थान पर राष्ट्रीय भावनाओं को मजबूत करने में सहायता की है लेकिन ये क्षेत्रीय भावनाओं को निर्मूल करने में कामयाब नहीं हो पायी हैं।
सामान्यतः देखा जाए तो क्षेत्रवाद का अर्थ सदैव पृथक्करण की भावना से नहीं होता बल्कि यदि यह सकारात्मक संतुलित विकास का दृष्टिकोण रखती है तो विकासात्मक अवधारणा है। क्षेत्रवाद का स्थायी समाधान लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में आर्थिक-सामाजिक एवं शैक्षिक विकास का प्रतिबद्ध विकेन्द्रीकरण है एवं स्वार्थगत क्षेत्रीय भावनाओं पर सख्त नियंत्रण है ताकि विघटनकारी तत्वों को समाप्त किया जा सके तथा साथ ही संतुलित, अखण्ड एवं अक्षुण्ण भारत स्थापित रहे।
समय रहते दलगत क्षेत्रीय उभार और उसके फैलाव को रोकने के लिए राष्ट्रीय दलों को पहले देश के हर कोने में रहने वालों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं ओ समझना होगा तथा उनकी आवाज बननी होगी। फिर राजनैतिक सौदेबाजी करने वालों को उन्हीं के क्षेत्र में बेनकाब करना होगा।
आर्थिक असमानता
आर्थिक असमानता का व्याप्त होना भी भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की स्थापना की दिशा में एक बड़ी बाधा है। यहां अभी भी एक ओर जहां 35 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गरीबी-रेखा के नीचे जीवन-यापन के लिए विवश है, तो दूसरी ओर 30 प्रतिशत शहरी आबादी सम्पूर भौतिक संसाधनों के साथ विलासितापूर्ण जीवन व्य्व्तित कर रहा है। पर्याप्त संसाधनों की उपस्थिति के बावजूद बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ओडीशा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों का आशा के अनुरूप आर्थिक विकास नहीं हो पाया है, जबकि एपेक्षक्रित कम संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों का पर्याप्त आर्थिक विकास हुआ है। पिछड़े राज्यों का मानना है कि ऐसा सरकार की दोषपूर्णदोहरी नीतियों के कारण ही हुआ है, इसलिए ये राज्य विकसित राज्यों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित नहीं कर पाए हैं।
भारत में विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिक संरचना भी ऐसी है कि धर्म, जाति, सम्प्रदाय तथा अमीर और गरीब का विभेद सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। संविधान के द्वारा सैद्धांतिक रूप से तो धर्मनिरपेक्षता और समानता के आदशों को स्थापित किया गया है, लेकिन व्यावहारिक रूप से अभी भी यहां धर्म-सापेक्षता और वर्गीय असमानता का वातावरण ही व्याप्त है।
उल्लिखित समस्याओं के अतिरिक्त भारत में राष्ट्र निर्माण की कुछ अन्य महत्वपूर्ण समस्याएं भी विद्यमान हैं। सबसे मुख्य चुनौती भारत की बहुजातीय, बहुधर्मीय, बहुनस्लीय, बहुभाषीय तथा बहुक्षेत्रीय जनसंख्या को एक एकीकृत राष्ट्रीय चेतना के आसपास समायोजित करके एक नयी राष्ट्रीय पहचान बनाने की है। आर्थिक असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, ग्रामीण-शहरी विभाजन, राजनीतिक लोकप्रियतावाद आदि भी राष्ट्र निर्माण के कार्य में बाधक हैं।
समस्या के निराकरण की युक्तियां
राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में आने वाली समस्याएं ज्ञात हैं, इसलिए उन्हें दूर करने के लिए सार्थक पहल की जा सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी भी भारत की आधी से अधिक जनसंख्या निरक्षर है। यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलीय प्रणाली अपनायी गयी है, परन्तु स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विरासत में मिली कांग्रेस पार्टी के अतिरिक्त कोई भी राजनीतिक दल लम्बी अवधि तक स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सका है; हमारे यहां अभी तक निष्पक्ष पत्रकारिता विकसित नहीं हो पायी है; प्रशासनिक व्यवस्था शिथिल है; आर्थिक असमानता व्याप्त ही है और अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी होती रही है।
किसी भी राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुरक्षित रखने के लिए वहां की जनता का शिक्षित होना नितांत आवश्यक होता है। जब तक कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को नहीं जानेगा, तब तक उसमें राष्ट्रीयता की भावना विकसित कैसे होगी। आज उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों की संख्या बहुत कम है और वे अपने निहित स्वार्थ के अनुरूप अशिक्षितों की भावनाओं को भड़काते हैं, परन्तु जब जनसंख्या का अधिकांश शिक्षित होगा, तब ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। इस समय हमारे देश की शिक्षा नीति भी दोषपूर्ण है, जिसके कारण अधिकांश लोग इससे दूर रहना चाहते हैं। अधिकांश परिवार ऐसे हैं, जो मुश्किल से एक शाम के भोजन का प्रबंध कर पाते हैं और वे अपने बच्चों को महंगाई के इस युग में शिक्षा दिलवा पाने में पूर्ण रूप से अक्षम हैं। नीति-निर्धारकों को ऐसी शिक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए, जो राष्ट्रीयता के हित में हो। केवल साक्षरता अभियानों से कुछ नहीं होने वाला-हस्ताक्षर मात्र का ज्ञान करा देना और अंकों का ज्ञान करा देना ही शिक्षा नहीं है। जन-साधारण में कम-से-कम इतनी चेतना का संचार करना तो नितांत आवश्यक है ही कि वे जान सकें कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। उनके भीतर जब तक इस चेतना का संचार नहीं होगा, तब तक वे देशभक्ति भी कोई चीज है, यह समझने में असमर्थ होंगे।
लोकतंत्र की मजबूती के लिए दलीय प्रणाली अच्छी समझी जाती है, परन्तु भारत में इनके निर्माण की स्वस्थ परम्परा विकसित नहीं हो सकी है, अपितु यहां कुकुरमुते की तरह राजनीतिक दलों का जन्म होने लगा है। ये सभी राजनीतिक दल सिद्धांतहीन राजनीति करते हैं और राष्ट्रीय हितों के ऊपर साम्प्रदायिक, जातिगत एवं भाषागत हितों को वरीयता देते हैं। प्रतिनिधि के चयन से लेकर मंत्रिमण्डल के गठन तक धर्म एवं जाति प्रभावी बने रहते हैं। भारत में क्षेत्रीय दलों का विकास और उनकी सुदृढ़ता भी खतरे का सूचक है, इसलिए राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को सिद्धांतों पर आधारित राजनीति का विकास करते हुए क्षेत्रीय दलों के प्रभाव में कमी लाने की दिशा में सार्थक पहल करनी चाहिए। जनता को भी चाहिए कि वह चुनावों के दौरान अपने मतों से उन्हीं प्रत्याशियों को चुने, जो राष्ट्रीय हित में कार्य करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हो। इसके लिए चुनाव आयोग तथा सरकार द्वारा भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है- उनके द्वारा साम्प्रदायिक तथा सिद्धांतहीन राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए तथा राजनीतिक दलों के लिए एक विस्तृत आचार संहिता बनायी जानी चाहिए। जो भी दल आचार संहिता का उल्लंघन करें, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए।
जब लोकतंत्र के तीनों स्थापित तंत्र- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने कार्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा नहीं रखते, तब चौथे स्वघोषित स्तम्भ पत्रकारिता की सक्रियता अपरिहार्य हो जाती है। वस्तुतः, पत्रकारिता एकमात्र ऐसी संस्था है, जिसका जन-साधारण के साथ वास्तविक रूप से प्रत्यक्ष संबंध रहता है। स्वस्थ जनता के निर्माण में पत्रकारिता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परन्तु, दुर्भाग्यवश भारत में पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं रह पायी है और न ही उसने अपने उत्तरदायित्व को ही पूरी तरह से निभाया है। पत्रकारिता ने हमारे देश में साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के पक्ष में प्रचार करने का कार्य ही अधिक किया है। जिन घटनाओं को प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं थी, उन घटनाओं की भी प्रकाशित कर जनता की उन्मादी भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है। यदि पत्रकारिता निष्पक्ष एवं उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका निभाए, तो राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण सहायता मिल सकती है।
भारत में प्रशासन की लापरवाही के कारण भी जातिगत तथा सम्प्रदायगत दंगों पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। अधिकारियों द्वारा सेवा में आगमन के समय निष्पक्षता की शपथ तो ली जाती है, किन्तु जब वे कार्य-क्षेत्र में जाते हैं, तब वे व्यवहार के समय सम्प्रदायगत एवं जातिगत विभेद की भावना से बच नहीं पाते हैं। जन-साधारण में सरकार के प्रति विश्वास जगाने के लिए प्रशासन को निष्पक्ष तथा उत्तरदायी बनाना नितांत आवश्यक है।
एकीकरण की स्थापना के लिए उठाए गए कदम
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए 1960 के दशक के पूर्वार्द्ध में प्रयत्न किए जाने लगे। 1961 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकीकरण समिति गठित की गई और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की व्यवस्था करना समिति का मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसी वर्ष 39 सदस्यीय एक राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया, जिसने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए अनेक सुझाव दिए। वर्ष 1963 में संविधान के अनुच्छेद 19 में संशोधन कर देश की प्रभुसत्ता और एकता को सुरक्षित करने के लिए विशेष परिस्थितियों में नागरिकों के स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों को सीमित करने का अधिकार सरकार को दिया गया। इसके साथ ही, भारतीय गणराज्य से अलगाव अथवा विघटनकारी प्रयत्न को अवैध और दण्डनीय अपराध के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद भी समय-समय पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता परिषद को पुनर्गठित किया गया और सभी अवसरों पर साम्प्रदायिकता से मुक्ति ही केंद्र-बिन्दु रही।
1996 में गठित संयुक्त मोर्चा सरकार के बाद देश में समान नागरिक संहिता की बात उठी है। संविधान के अनुच्छेद 44 में देश के सभी भागों, सभी नागरिकों के लिए एक प्रकार की विधि के निर्माण का उपबंध है परन्तु, मुस्लिमों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने भी 1985 में जॉर्डन बनाम चोपड़ा के मामले में यह स्पष्ट किया कि, समान नागरिक संहिता से राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा और ऐसी विधियां समाप्त हो जाएंगी, जिनके आदर्श परस्पर विरोधी हैं।
राष्ट्रीय एकीकरण केवल सरकारी प्रयत्न से संभव नहीं है, इसके लिए सर्वसाधारण का प्रयत्न आवश्यक है- विभिन्न सम्प्रदायों को, विभिन्न जातियों को, विभिन्न भाषायी समूहों को और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आपसी मतभेद को भुलाकर एक राष्ट्र के समस्त निवासी की भावना से कार्य करना होगा तथा राष्ट्र की एकता और अखण्डता को कायम रखने के लिए सम्मिलित प्रयत्न करना होगा।