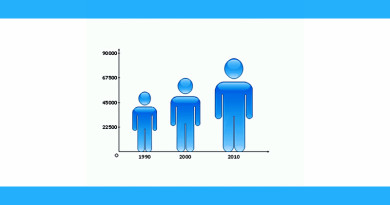स्वतंत्रता पश्चात् भारत में योजना व्यवस्था Planning System After Independence In India
दीर्घकालीन औपनिवेशिक शासन के फलस्वरूप भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली, जिसमें सीमित उद्योगीकरण, निम्न कृषि उत्पादन, अल्प प्रति व्यक्ति आय तथा मंद आर्थिक विकास गति जैसी नकारात्मक विशेषताएं मौजूद थी। अशिक्षा, संकीर्णता तथा सामाजिक असमानता इसके अन्य प्रमुख तत्व थे।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनितिक नेतृत्व द्वारा परिस्थितियों एवं जनाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विकास के चार लक्ष्य घोषित किये गये, ये थे-
- आयात और विदेशी सहायता पर भारत की निर्भरता को कम करना
- पूंजी निर्माण एवं संसाधनों का प्रसार करना
- सामाजिक एवं क्षेत्रीय असमानताओं का उन्मूलन करना, तथा
- जनसामान्य हेतु पर्याप्त एवं न्यूनतम जीवन स्तर की उपलब्धि करना|
उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राजनीतिक नेतृत्व के पास दो विचारधाराओं- पूंजीवादी और साम्यवादी पर आधारित शासन प्रणालियों को अपनाने के विकल्प मौजूद थे, किंतु पूंजीवादी व्यवस्था में व्याप्त असमानता तथा साम्यवादी शासन की निरंकुशता ने भारतीय नेतृत्व को तीसरे रास्ते का चुनाव करने को प्रेरित किया। जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक नियोजन को लागू करने के नये प्रयोग को अपनाने का निर्णय किया गया, जिसमें विकास और समता के उद्देश्यों को शांतिपूर्ण तरीके से प्राप्त किया जाना था।
[divide]
नियोजन सम्बंधी प्रारंभिक प्रयास
कांग्रेस ने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू थे। समिति द्वारा तैयार कई रिपोर्टों में मूलभूत उद्योगों के सार्वजानिक स्वामित्व, बड़े और लघु उग्योगों के मध्य समन्वय, क्षतिपूर्ति देकर जमीदारी प्रथा के उन्मूलन, नियोजन में कृषि क्षेत्र को आवश्यक रूप से शामिल करने तथा सहकारी खेती के विस्तार आदि की सिफारिशें कीं गयीं।
1944 में भारत के आठ बड़े उद्योगपतियों ने आर्थिक विकास का एक दस्तावेज तैयार किया जिसे बंबई योजना कहा जाता है।
आचार्य श्री मन्नारायण द्वारा ‘गांधीवादी योजना‘ के माध्यम से दस वर्ष में लोगों को जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया गया। एम.एन. राय ने भी ‘जनता योजना‘ का प्रस्ताव रखा, जिसमें सरकारी खेती और भूमि के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया गया। जयप्रकाश नारायण की ‘सर्वोदय योजना‘ भी विकास के गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी।
इस प्रकार विकास की इन विभिन्न योजनाओं के द्वारा भारत में नियोजन के कई प्रारूप उभर कर आये, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीतिक नेतृत्व को नियोजन सम्बंधी नीतिनिर्माण हेतु प्रचुर आधार-सामग्री उपलब्ध करायी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। आयोग को परामर्शदात्री संस्था का दर्जा दिया गया। आयोग को सात दायित्व निभाने थे-
- भारत के भौतिक, पूंजीगत तथा मानवीय संसाधनों का आंकलन करना;
- इन संसाधनों के प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना;
- विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित करना, विकास की स्थितियों को परिभाषित करना तथा संसाधनों के वितरण हेतु सुझाव देना;
- योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक शतों का निर्धारण करना;
- योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित प्रशासतंत्र सुनिश्चित करना;
- योजना क्रियान्वयन द्वारा हासिल प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन करना तथा नीतियों और मापदंडों में अपेक्षित सुधारों की सिफारिश करना;
- स्वयं की प्रभावी कार्यशीलता, बदलती आर्थिक परिस्थितियों, चालू समस्या आदि विषयों के सम्बंध में अपनी सिफारिशें देना।
योजना आयोग की सिफारिशों तथा तैयार नीतियों व योजनाओं पर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं।
[divide]
नियोजन के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य Planning, Socio-Economic Objective
नियोजन के विभिन्न सामाजिक आर्थिक उद्देश्य हैं, जिन्हें विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूपों में वर्णित किया जाता रहा है। एक मोटे अनुमान के आधार पर नियोजन के उद्देश्य निम्न हैं-
- आधारभूत औद्योगिक संरचना का निर्माण;
- कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं सुधार;
- राष्ट्रीय संपदा की वृद्धि और वितरण;
- आत्म निर्भर और स्वस्फूर्त राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना;
- गरीबी व बेरोजगारी का उन्मूलन
- सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन;
- बीमारियों और निरक्षरता की समाप्ति;
- व्यापार और वाणिज्य का विस्तार;
- आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यातोन्मुख उत्पादन हेतु उद्यमियों को आर्थिक प्रोत्साहन;
- भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिक, प्रभावशील व प्रतिस्पद्धत्मिक रूप में कायांतरण।
[divide]
पहली तीन पंचवर्षीय योजनाएं The First Three, Five-Year Plans
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56): प्रथम योजना में सवांगीण राष्ट्रीय विकास के साथ-साथ शरणार्थी पुनर्वास, खाद्य आत्मनिर्भरता, मुद्रास्फीति नियंत्रण जैसे तात्कालिक लक्ष्यों का चुनाव किया गया। इस योजना को लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त हुई।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61): इस योजना में भारी एवं मूलभूत उद्योगों के विकास एवं विस्तार को प्राथमिकता दी गयी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था।
दूसरी योजना के अनेक लक्ष्यों को पूंजी अभाव के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका, फिर भी इसे सीमित सफलता प्राप्त हुई।
तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66): तीसरी योजना में कृषि को पुनः सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्वस्फूर्त एवं निर्भर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया गया। किंतु भारत-चीन युद्ध (1962) तथा भारत-पाकिस्तान युद्ध (1965) के कारण योजना की प्राथमिकताओं को रक्षा जरूरतों तक सीमित होना पड़ा। 1965-66 में पड़े भयंकर अकाल ने पूरी तरह इस योजना को विफल बना दिया। अतः तीसरी योजना के दौरान भारतीय नियोजन प्रणाली को गंभीर संकटों व अवरोधों का सामना करना पड़ा।
इस प्रकार जवाहर लाल नेहरू के कार्यकाल में ही नियोजन व्यवस्था के सकारात्मक एवं नकारात्क पहलू पूर्णतः स्पष्ट हो गये। जहां एक ओर उत्पादन वृद्धि औद्योगीकरण विस्तार, आधार संरचना विकास, विज्ञान एवं तकनीकी विकास, तथा शिक्षा के प्रसार आदि क्षेत्रों में नियोजन प्रणाली को सफलता प्राप्त हुई, वहीं दूसरी ओर गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन, आय असमानताओं में कमी, भूमिसुधारों के पूर्ण क्रियान्वयन आदि क्षेत्रों में यह असफल साबित हुई।
[divide]
राज्य नियंत्रित औद्योगीकरण State-Controlled Industrialization
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के औद्योगीकरण क्षेत्र में आधारभूत संरचना का आभाव, तकनीकी विकास की निम्न स्थिति, विदेशी पूंजी पर निर्भरता, घरेलू बाजार की अनुपस्थिति, पूंजीगत उद्योगों का आभाव तथा पूंजी निर्माण की कमी जैसी विशेषताएं विद्यमान थीं। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व तथा उद्यमियों द्वारा औद्योगीकरण के विकास व विस्तार के लिए आधारभूत संरचना, घरेलू मांग तथा विशेष योग्य संसाधनों की उपलब्धता को अनिवार्य शतों के रूप में स्वीकार किया गया और इन शर्तों को राजकीय सहयोग के बिना पूरा करना असंभव समझा गया।
1938 की ‘राष्ट्रीय योजना समिति’ तथा 1944 की बंबई योजना द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को गतिशील बनाने के लिए नियोजन प्रणाली तथा राज्य नियंत्रण की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था।
लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों को औद्योगीकरण के माध्यम से प्राप्त करने के लिए भी उद्योगों पर सरकारी स्वामित्व कायम रखना जरूरी था। निजी क्षेत्र के अधिकाधिक लाभार्जन करने के दृष्टिकोण के कारण उससे सामाजिक कल्याण से संबंधित प्रायमिकताओं की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। धन अंकुश रखना उचित समझा गया। औद्योगीकरण पर राज्य नियंत्रण के स्वरूप को सरकार की आरंभिक औद्योगिक नीतियों में देखा जा सकता है।
[divide]
1948 की औद्योगिक नीति Industrial Policy of 1948
इस नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आगामी वर्षों में राज्य द्वारा अपने नियंत्रणाधीन नवीन उत्पादक इकाइयों की स्थापना की घोषणा की गई। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र को संयुक्त रूप से कार्य करना था। निजी क्षेत्र को देश की सामान्य औद्योगिक नीति के अंतर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करनी थीं। ऊर्जा, शस्त्रास्त्र, रेलवे, मुद्रा उत्पादन आदि क्षेत्रों में राज्य के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की परिकल्पना की गई। विमान एवं पोत निर्माण, लोहा, कोयला खनिज तेल तथा संचार क्षेत्र में राज्य द्वारा आधारभूत उद्योगों की स्थापना करने का निश्चय किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र को सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में मान्यता दी गयी। इस नीति में लघु एवं कुटीर उद्योगों को राज्य द्वारा प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव था। इन उद्योगों हेतु विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन को आरक्षित किया गया। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना भी राज्य का दायित्व माना गया। इस प्रकार 1948 की औद्योगिक नीति द्वारा संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया गया।
[divide]
1956 की औद्योगिक नीति Industrial Policy of 1956
इस नीति के प्रस्ताव में उद्योगों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया-
- पहले वर्ग में शस्त्रास्त्र उत्पादन, परमाणु उर्जा, भारी उपकरण, लौह इस्पात, कोयला, खनिज तेल, धातु उद्योग, भारी विद्युत् उपकरण, अन्य महत्त्व खनिज वायु परिवहन, रेलवे, वैमानिकी टेलीफोन, विद्युत् उत्पादन व् वितरण तथा टार एवं रेडियो उपकरण जैसे 17 उद्योगों को रखा गया। ये राज्य के पूर्ण नियंत्रण में थे।
- दूसरे वर्ग में अन्य अलौह धातु व एल्यूमिनियम, अन्य खनिज उद्योग, लौह मिश्रधातु एवं इस्पात, प्रतिजैविक व् अन्य औषधि, रसायन उद्योग, उर्वरक, संश्लिष्ट रबर, सड़क परिवहन व समुद्री परिवहन, कोयले का कार्बनीकरण तथा रासायनिक अपशिष्ट जैसे 12 उद्योगों को शामिल किया गया। इन उद्योगों में राज्य का नियंत्रण बढ़ता जाना था तथा राज्य इनमें नवीन उद्यमों की स्थापना करेगा। निजी क्षेत्र से इन उद्योगों के संचालन में राज्य की सहायता करने की अपेक्षा की गई।
- शेष सभी उद्योग निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप दिये गये। किंतु इस वर्ग के सभी उद्योगों को भी सामाजिक उद्देश्यों एवं नियंत्रक विधानों के अधीन कार्य करना था।
इस औद्योगिक नीति में स्पष्ट किया गया कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र आपस में पृथक या विरोधी नहीं बल्कि परस्पर पूरक है। निजी क्षेत्र की आशंका का समाधान करने के लिए राज्य द्वारा पूंजी का समर्थन, राजकोषीय उपायों तथा संचार व ऊर्जा सुविधाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र के विकास को पर्याप्त समर्थन दिया गया। नीति में राज्य के, सरकारी व निजी दोनों इकाइयों के प्रति न्यायपूर्ण एवं भेदभाव रहित व्यवहार को सुनिश्चित किया गया। इसमें लघु व कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन, प्रादेशिक असमानता की समाप्ति तथा श्रमिक सुविधाओं के विस्तार की सिफारिशें भी की गयी, जिन्हें पूरा करना राज्य के नियंत्रण के बगैर असंभव था।
[divide]
प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन औद्योगीकरण
प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत औद्योगीकरण, 1951-56 Industrialization Under The First Five-Year Plan, 1951-56
प्रथम योजना में प्रत्यक्ष औद्योगीकरण प्रयासों की बजाय आधारभूत सरंचना एवं कृषि एवं सिंचाई के विकास पर जोर दिया गया ताकि आगामी समय में किये जाने वाले तीव्र औद्योगीकरण हेतु सुगम पृष्ठभूमि निर्मित की जा सके। विभिन्न उद्योगों की विकास दर प्रथम योजना काल में संतोषजनक रही। इसी काल में सिंदरी उर्वरक कारखाना, चितरंजन का रेल इंजन निर्माण कारखाना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेनिसिलीन फैक्ट्री, भारतीय टेलीफोन उद्योग आदि की स्थापना की गई।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत औद्योगीकरण, 1956-61 Industrialization Under The Second Five-Year Plan, 1956-61
इस योजनाकाल में निर्धारित औद्योगीकरण का लक्ष्य, 1956 की औद्योगिक नीति से प्रेरित था। योजना के कुल विनियोग का 27 प्रतिशत अंश उद्योग क्षेत्र के लिए निश्चित किया गया। राज्य द्वारा राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर स्थित इस्पात कारखानों के अतिरिक्त विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में अनेक उत्पादक इकाइयां स्थापित की गयीं। इस काल में छोटे उद्यमकर्ता समूह का तेजी से विस्तार हुआ, जिससे पूंजी एकाधिकार की प्रवृत्तियों में आंशिक रूप से कमी आयी।
तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत औद्योगीकरण, 1961-66 Industrialization Under The Third Five-Year Plan, 1961-66
इस योजनाकाल में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ मशीन निर्माण उत्पादन, तकनीकी कौशल एवं प्रबंधकीय दक्षता में सुधार करने पर बल दिया गया। योजनाकाल के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र को केंद्रीय स्थान प्रदान किया गया। योजनाकाल के दौरान ओटोमोबाइल, दीजल इंजन, बिजली ट्रांसफार्मर, मशीनी उपकरण आदि क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई।
[divide]
उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 The Industries (Development and Regulation) Act, 1951
इस अधिनियम के माध्यम से सरकार को मध्यम एवं बड़े औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। सरकार को उत्पादन की मात्र, आयात-निर्यात कोटा, मजदूरी, मूल्य एवं वेतन के निर्धारण की शक्ति भी प्राप्त हुई। सरकार के इन अधिकारों को उद्योगों के विकेंद्रीकरण तथा उपभोक्ता व श्रमिकों के हित संरक्षण की दृष्टि से औचित्यपूर्ण सिद्ध किया गया। सरकार द्वारा विदेशी व्यापार घरानों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों को भी विभिन्न कानूनों के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास किया गया।
इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के डेढ़ दशक में लोकतांत्रिक समाजवाद के आदशों के अनुरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगीकरण की जो प्रक्रिया आरंभ की गयी, उसमें राज्य के नियंत्रण को अनिवार्य तत्व माना गया। तत्कालीन नवीन अर्थव्यवस्था में आधारभूत क्षेत्रों को मात्र निजी एवं बाजारवादी आर्थिक शक्तियों के सहारे विकसित करना असंभव था और स्वयं निजी क्षेत्र भी इतना सामर्थ्यवान नहीं हो पाया या जो सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्सरचना हेतु अपेक्षित संसाधनों को जुटा सकने में समर्थ हो पाता। राज्य नियंत्रण के माध्यम से ही कृषि, ऊर्जा, परिवहन तथा संचार क्षेत्र में संसाधनों का निवेश सुनिश्चित किया जा सकता था। इन आधारभूत सुविधाओं के विकास के बिना घरेलू बाजार का निर्माण तथा सामाजिक परिवर्तन का होना संभव नहीं था। इन सब कारणों से राज्य को औद्योगीकरण प्रक्रिया के नियंत्रण की बागडोर सौंपी गयी और कतिपय असफलताओं के बावजूद राज्य द्वारा अपनी भूमिका को कुशलतापूर्वक निभाया गया ।
[divide]
कृषिक सुधार, 1947-64 Agricultural Reform, 1947-64
स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत राजनैतिक नेतृत्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती देश का सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास करने की थी। भारत की 80 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या की आजीविका कृषि पर निर्भर होने के कारण कृषि को आर्थिक विकास से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध पाया गया। आजादी के बाद भारत को पिछड़ी हुई कृषि व्यवस्था विरासत में प्राप्त हुई, जिसके मुख्य लक्षण इस प्रकार थे- भूस्वामित्व के विभिन्न प्रकार, कुछ गिने-चुने हाथों में भूमि का केन्द्रीकरण, बिचौलियों की प्रभावशीलता, बहुसंख्यक गरीब किसानों का अस्तित्व, ग्रामीण बेरोजगारी, न्यून कृषि, उत्पादन, तकनीकी सुविधाओं का आभाव, सामाजिक पिछड़ापन एवं भेदभाव, निम्न ग्रामीण जीवन स्तर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता, रूढ़िवाद, धर्मांधता व जातिवाद का वर्चस्व आदि।
स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण जीवन और कृषि में सुधार करना नेतृत्व की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर था। तत्कालीन समय में कृषि सुधार से जुड़ी तीन विचारधाराएं मौजूद थीं-
- भारतीय साम्यवादी दल द्वारा भूमि के राष्ट्रीयकरण को अनिवार्य माना गया।
- विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के अंतर्गत भूमि सुधारों की नैतिक दबाव के आधार पर तय करने का आह्वान किया गया।
- 1949 में कांग्रेस कृषि सुधार समिति के प्रतिवेदन में संघीय लोकतांत्रिक ढांचे के अधीन भूमि सुधार तथा सहकारी खेती पर बल दिया गया। पहली दो विचारधाराओं को कानूनी समर्थन के अभाव में अस्वीकार कर दिया गया तथा कांग्रेस की नीतियों के आधार पर ही कृषि सुधारों की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का निश्चय किया गया।
1955 के आवड़ी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा समाजवादी ढांचे के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधारों के निम्न उद्देश्य निश्चित किये गये-
- ग्रामीण भारत में प्रभावी अर्धसामंती सामाजिक सम्बंधों तथा आर्थिक संस्थाओं का उन्मूलन;
- वास्तविक किसानों को भूमि का वितरण;
- सरकारी सामुदायिक विकास योजनाओं द्वारा प्रगतिशील किसानों की क्षमता में वृद्धिः
- खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि;
- काश्तकारी अवधि की सुरक्षा सुनिश्चित करना;
- लगान का भुगतान नकदी में करना
इन उद्देश्यों की प्राप्ति संसदीय लोकतंत्र के अधीन तथा सम्पति के अधिकार को बिना क्षति पहुंचाये, की जानी थी। भारतीय संसद द्वारा भी शीघ्र ही कांग्रेस के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया।
[divide]
प्रथम चरण 1948-52
इस चरण सरकार द्वारा जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन पर अधिक बल दिया गया जिससे बिचौलियों को समाप्त करके कृषकों के साथ सीधा सम्पर्क कायम किया जा सके। काश्तकार की वैधानिक परिभाषा में लघु किसानों के साथ-साथ बड़े-बड़े भूस्वामियों को भी शामिल किया गया। कृषि श्रम जांच रिपोर्ट (1951) के अनुसार “कुल कृषक परिवारों में 20 प्रतिशत लोग भूमिहीन थे। 2.5 एकड़ से कम भूमि प्राप्त किसानों का प्रतिशत 38 था और कुल खेती योग्य भूमि के मात्र 6 प्रतिशत पर ही उनका अधिकार था।। 59 प्रतिशत कृषक परिवारों के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि थी जो कुल खेती योग्य भूमि का 16 प्रतिशत थी।”
आजादी के समय व्यक्तिगत स्वामित्व की 57 प्रतिशत कृषि भूमि पर जमीदारों का प्रभुत्व था। सरकार द्वारा जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कदम उठाये जाने पर निम्न कठिनाइयां उपस्थित हुई-
- कृषि राज्य सूची का विषय था। अतः इस दिशा में किया गया कोई भी सुधार संपूर्ण भारत में एक साथ लागू करना अत्यंत दुष्कर था। विभिन्न राज्यों की भू-सुधार नीतियों में विभिन्नता थी।
- खेतिहर व सीमांत कृषकों को राज्य के प्रत्यक्ष सम्पर्क में लाना एक विकट समस्या थी।
- अधिग्रहीत की गई भूमि के बदले मुआवजा देना भी एक समस्या थी। जमींदार मुआवजे के प्रश्न को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय से असंवैधानिक घोषित करा लेते थे। अनुच्छेद 31 में संशोधन करके ही भूमि सुधारों को लागू किया जा सका। जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के बाद भी जमीदारों को “भू-कृषक’ का दर्जा प्रदान किया गया तथा उन्हें निजी खेती के लिए भूमि के पुनग्रहण की सुविधा भी दी गई।
काश्तकारों को भूमि जोतने का स्थायी अधिकार दे दिया गया किंतु वे जमीन का विक्रय नहीं कर सकते थे। एक वर्ष के लगान का दस गुना अदा करने वाले काश्तकार ही भूमि को बेच सकते थे। इस प्रकार अधिकांश किसान भूमिधर और सिरदार के रूप में बदल गये, जो सरकार को सीधे लगान देते थे। किंतु जमीदारों पर अभी भी खुदकाश्त के रूप में काफी भूमि बची रह गयी थी और सरकार से प्राप्त मुआवजे को लाभकारी व्यवसायों में नियोजित करके उन्होंने अपनी प्रभावपूर्ण सामाजिक व आर्थिक स्थिति को पूर्णतः समाप्त नहीं होने दिया था।
[divide]
द्वितीय चरण 1951-64
इस चरण में कृषिक सुधारों के अंतर्गत अनेक वैधानिक कदम उठाये गये। काश्तकारी अवधि की सुरक्षा, लगान दर के निर्धारण, तथा काश्तकारों को भूमि खरीद कर स्वामी बनने का अवसर देने के उद्देश्य से कई कानून बनाये गये। कृषि भूमि की सीमा तथा भूमिहीनों को कृषि भूमि के वितरण के संबंध में भी कई कानून बनाये गये। छठे दशक के प्रारंभिक वर्षों में योजना आयोग द्वारा एक पारिवारिक जीत का निर्धारण किया गया, जिसकी वार्षिक आमदनी 1200 रु. के बराबर हो। योजना आयोग द्वारा दिये गये सुझाव में 5 सदस्यीय परिवार के पास 3 पारिवारिक जोतों के स्वामित्व की जरूरी माना गया। प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं के प्रपत्रों में भी काश्तकारों की दशा सुधारने के संबंध में निम्न प्रस्ताव मौजूद थे-
- भूमि का किराया कुल उत्पादन के 1/2 से 1/4 स्तर से ज्यादा न हो;
- जिस भूमि के पुनग्रहण की संभावना न हो, उसका स्वामित्व काश्तकार को सौंपा जाये;
- दूरस्थ जमींदारी को हतोत्साहित किया जाये;
- व्यक्तिगत कृषि को प्रोत्साहन दिया जाये।
इन पंचवर्षीय योजनाओं में असमानता की समाप्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता को स्वीकार किया गया। भूमि हदबंदी कानून 1950 के दशक में ही लागू हो गया किंतु उसका क्रियान्वयन विभिन्न राज्यों में अलग-अलग समय पर हुआ। भूमि हदबंदी के उद्देश्य को आंशिक सफलता ही मिल सकी क्योंकि भूमिपतियों ने अपनी अधिशेष भूमि अपने रिश्तेदारों, मित्रों व अन्य लोगों के नाम कर दी थी। इस बेनामी हस्तांतरण ने भूमि हदबंदी कानूनों को एक सीमा तक अप्रभावी बना दिया।
कृषि सुधारों के अंतर्गत भारी निवेश के द्वारा भूमि की उत्पादकता’ बढ़ने पर भी जोर दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि चकबंदी की व्यवस्थित शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य भूमि के उपविभाजन को रोकना था। 1957 के अंत तक 150 लाख एकड़ भूमि की चकबंदी हो चुकी थी। भूमि सुधारों के साथ ही संविधान के निर्देशक तत्वों (अनुच्छेद 40) के अधीन, ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू की गयी, जो वयस्क और व्यापक मताधिकार पर आधारित थी। ग्रामीण पंचायतों द्वारा ग्रामीण स्तर के भूमि संसाधनों के नियंत्रण से ग्रामीण जीवन में एक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की शुरुआत हुई।
कृषिक सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए भी कई प्रयास किये। 1960 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम को कुछ राज्यों के चयनित जिलों में लागू किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां, अच्छे बीज तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना था। इन सुविधाओं के साथ-साथ सिंचाई की उचित व्यवस्था पर भी बल दिया गया।
किंतु इन सुविधाओं का सर्वाधिक लाभ अमीर कृषकों द्वारा उठाया गया। यद्यपि इससे सरकार को उत्पादन में वृद्धि हासिल करने में सफलता प्राप्त हुई किंतु कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन तथा सामाजिक-आर्थिक समानता लाने के प्रयासों को कई अवरोधों का सामना करना पड़ा।
निष्कर्ष रूप में 1947-64 के काल में कृषिक सुधारों को लागू करने के अभूतपूर्व प्रयास किये गये किंतु वे कृषि क्षेत्र में आमूल संरचनात्मक परिवर्तन लाने में अपर्याप्त रहे, जिसका कारण मूलतः तत्कालीन सामाजिक-आर्थिक संरचना में निहित था।